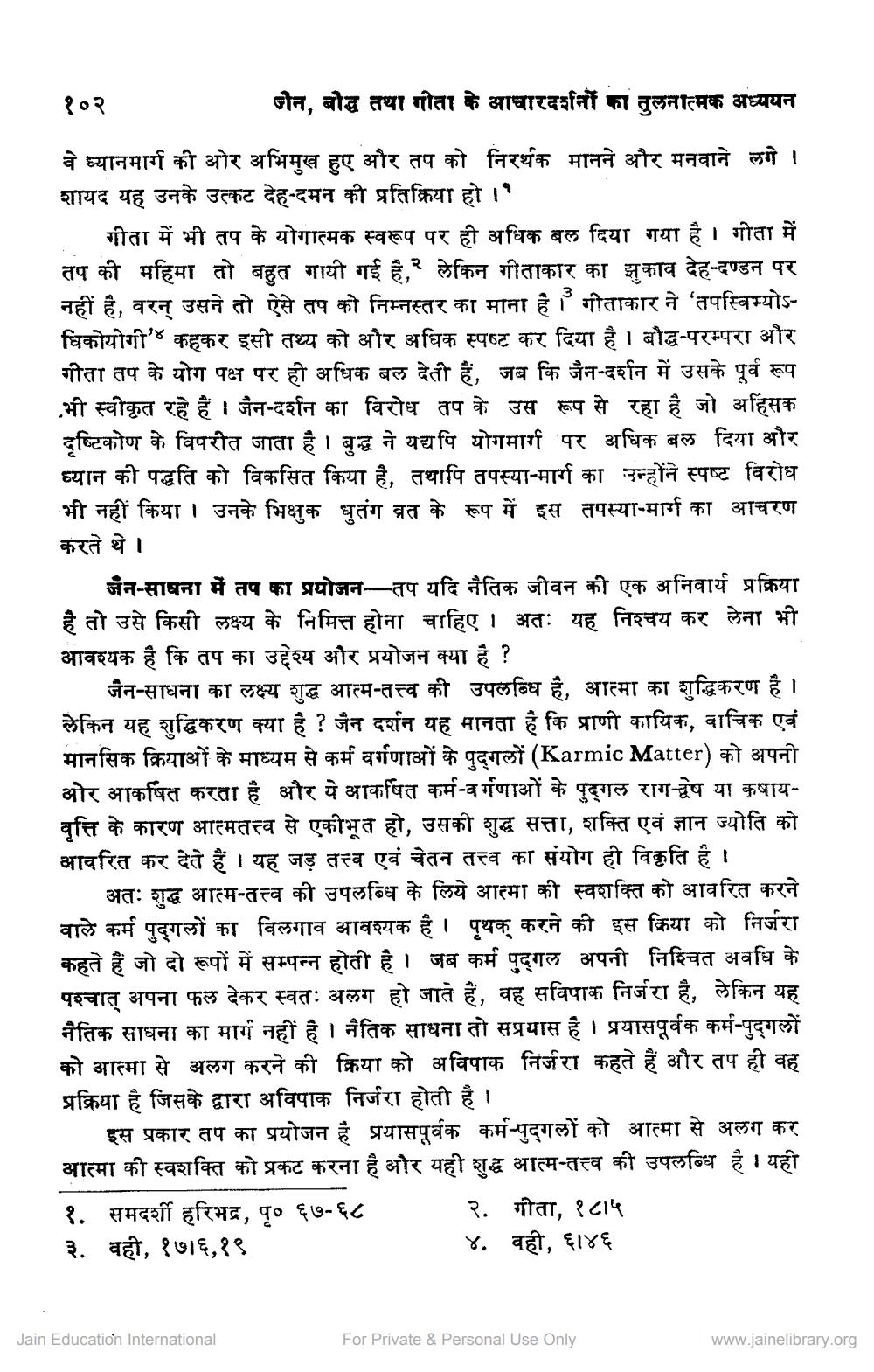________________
१०२
जैन, बौद्ध तथा गीता के आधारदर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन वे ध्यानमार्ग की ओर अभिमुख हुए और तप को निरर्थक मानने और मनवाने लगे । शायद यह उनके उत्कट देह-दमन की प्रतिक्रिया हो ।'
गीता में भी तप के योगात्मक स्वरूप पर ही अधिक बल दिया गया है । गीता में तप की महिमा तो बहुत गायी गई है, लेकिन गीताकार का झुकाव देह-दण्डन पर नहीं है, वरन् उसने तो ऐसे तप को निम्नस्तर का माना है। गीताकार ने 'तपस्विभ्योऽधिकोयोगी' कहकर इसी तथ्य को और अधिक स्पष्ट कर दिया है । बौद्ध-परम्परा और गीता तप के योग पक्ष पर ही अधिक बल देती हैं, जब कि जैन-दर्शन में उसके पूर्व रूप भी स्वीकृत रहे हैं । जैन-दर्शन का विरोध तप के उस रूप से रहा है जो अहिंसक दृष्टिकोण के विपरीत जाता है । बुद्ध ने यद्यपि योगमार्ग पर अधिक बल दिया और ध्यान की पद्धति को विकसित किया है, तथापि तपस्या-मार्ग का उन्होंने स्पष्ट विरोध भी नहीं किया। उनके भिक्षुक धुतंग व्रत के रूप में इस तपस्या मार्ग का आचरण करते थे।
जन-साधना में तप का प्रयोजन-तप यदि नैतिक जीवन की एक अनिवार्य प्रक्रिया है तो उसे किसी लक्ष्य के निमित्त होना चाहिए । अतः यह निश्चय कर लेना भी आवश्यक है कि तप का उद्देश्य और प्रयोजन क्या है ?
जैन-साधना का लक्ष्य शुद्ध आत्म-तत्त्व की उपलब्धि है, आत्मा का शुद्धिकरण है। लेकिन यह शुद्धिकरण क्या है ? जैन दर्शन यह मानता है कि प्राणी कायिक, वाचिक एवं मानसिक क्रियाओं के माध्यम से कर्म वर्गणाओं के पुद्गलों (Karmic Matter) को अपनी ओर आकर्षित करता है और ये आकर्षित कर्म-वर्गणाओं के पुद्गल राग-द्वेष या कषायवृत्ति के कारण आत्मतत्त्व से एकीभूत हो, उसकी शुद्ध सत्ता, शक्ति एवं ज्ञान ज्योति को आवरित कर देते हैं । यह जड़ तत्त्व एवं चेतन तत्त्व का संयोग ही विकृति है ।।
अतः शुद्ध आत्म-तत्त्व की उपलब्धि के लिये आत्मा की स्वशक्ति को आवरित करने वाले कर्म पुद्गलों का विलगाव आवश्यक है। पृथक् करने की इस क्रिया को निर्जरा कहते हैं जो दो रूपों में सम्पन्न होती है। जब कर्म पुद्गल अपनी निश्चित अवधि के पश्चात् अपना फल देकर स्वतः अलग हो जाते हैं, वह सविपाक निर्जरा है, लेकिन यह नैतिक साधना का मार्ग नहीं है । नैतिक साधना तो सप्रयास है । प्रयासपूर्वक कर्म-पुद्गलों को आत्मा से अलग करने की क्रिया को अविपाक निर्जरा कहते हैं और तप ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अविपाक निर्जरा होती है ।
इस प्रकार तप का प्रयोजन है प्रयासपूर्वक कर्म-पुद्गलों को आत्मा से अलग कर आत्मा की स्वशक्ति को प्रकट करना है और यही शुद्ध आत्म-तत्त्व की उपलब्धि है । यही १. समदर्शी हरिभद्र, पृ० ६७-६८ २. गीता, १८१५ ३. वही, १७१६,१९
४. वही, ६।४६
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org