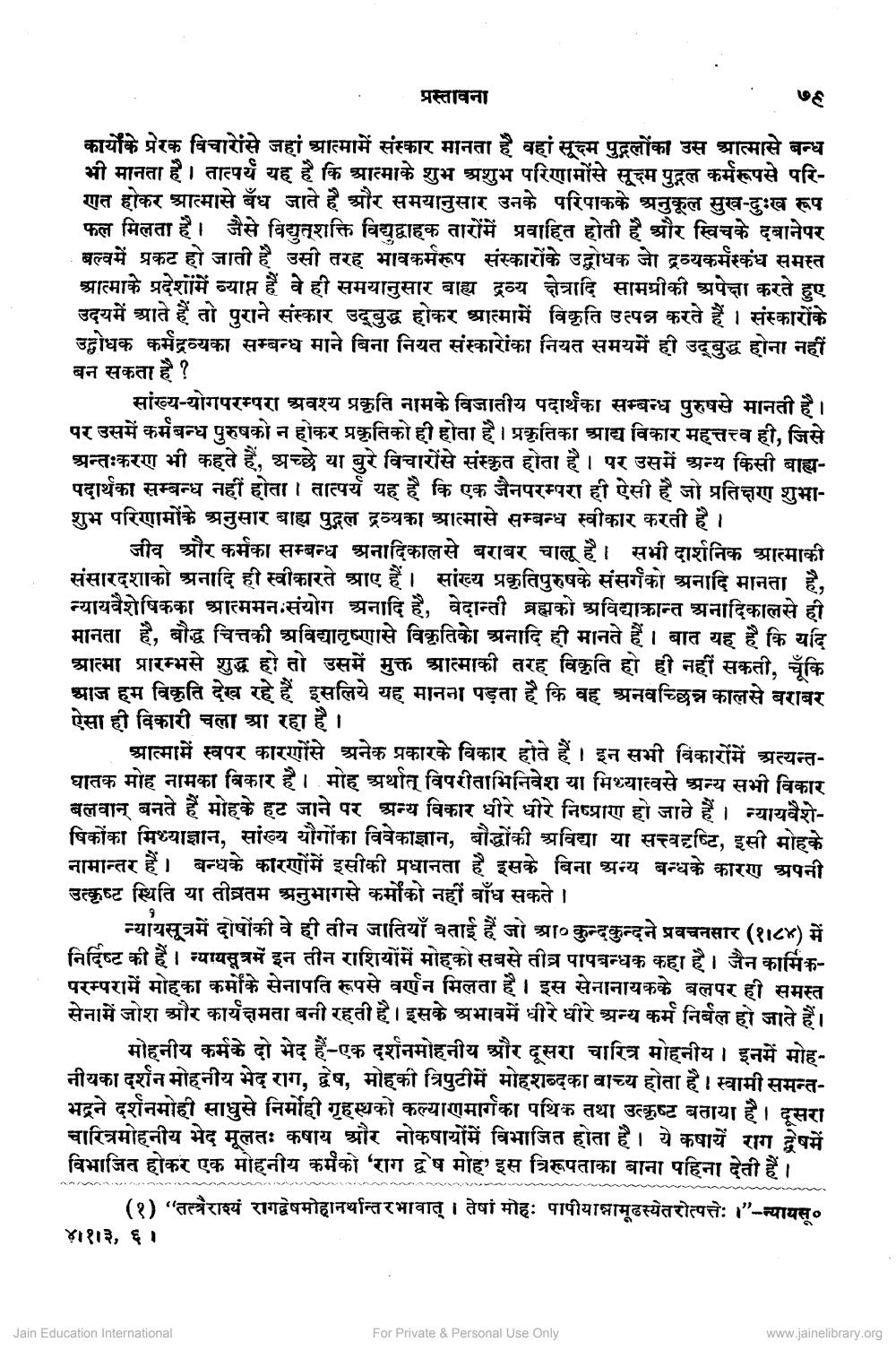________________
प्रस्तावना
कार्योंके प्रेरक विचारोंसे जहां आत्मामें संस्कार मानता है वहां सूक्ष्म पुद्गलोंका उस आत्मासे बन्ध भी मानता है। तात्पर्य यह है कि आत्माके शुभ अशुभ परिणामोंसे सूक्ष्म पुद्गल कर्मरूपसे परिणत होकर आत्मासे बँध जाते है और समयानुसार उनके परिपाकके अनुकूल सुख-दुःख रूप फल मिलता है। जैसे विद्युत्शक्ति विद्युद्वाहक तारोंमें प्रवाहित होती है और स्विचके दबानेपर बल्वमें प्रकट हो जाती है उसी तरह भावकर्मरूप संस्कारोंके उद्बोधक जो द्रव्यकर्मस्कंध समस्त आत्माके प्रदेशों में व्याप्त हैं वे ही समयानुसार बाह्य द्रव्य क्षेत्रादि सामग्रीकी अपेक्षा करते हुए उदयमें आते हैं तो पुराने संस्कार उबुद्ध होकर श्रात्मामें विकृति उत्पन्न करते हैं। संस्कारोंके उद्धोधक कर्मद्रव्यका सम्बन्ध माने बिना नियत संस्कारोंका नियत समयमें ही उबुद्ध होना नहीं बन सकता है ?
सांख्य-योगपरम्परा अवश्य प्रकृति नामके विजातीय पदार्थका सम्बन्ध पुरुषसे मानती है। पर उसमें कर्मबन्ध पुरुषको न होकर प्रकृतिको ही होता है। प्रकृतिका आद्य विकार महत्तत्त्व ही, जिसे अन्तःकरण भी कहते हैं, अच्छे या बुरे विचारोंसे संस्कृत होता है। पर उसमें अन्य किसी बाह्यपदार्थका सम्बन्ध नहीं होता। तात्पर्य यह है कि एक जैनपरम्परा ही ऐसी है जो प्रतिक्षण शुभाशुभ परिणामोंके अनुसार बाह्य पुद्गल द्रव्यका आत्मासे सम्बन्ध स्वीकार करती है।
जीव और कर्मका सम्बन्ध अनादिकालसे बराबर चालू है। सभी दार्शनिक आत्माकी संसारदशाको अनादि ही स्वीकारते आए हैं। सांख्य प्रकृतिपुरुषके संसर्गको अनादि मानता है, न्यायवैशेषिकका आत्ममनःसंयोग अनादि है, वेदान्ती ब्रह्मको अविद्याक्रान्त अनादिकालसे ही मानता है, बौद्ध चित्तकी अविद्यातृष्णासे विकृतिको अनादि ही मानते हैं। बात यह है कि यदि आत्मा प्रारम्भसे शुद्ध हो तो उसमें मुक्त आत्माकी तरह विकृति हो ही नहीं सकती, चूंकि आज हम विकृति देख रहे हैं इसलिये यह मानना पड़ता है कि वह अनवच्छिन्न कालसे बराबर ऐसा ही विकारी चला आ रहा है।
आत्मामें स्वपर कारणोंसे अनेक प्रकारके विकार होते हैं। इन सभी विकारोंमें अत्यन्तघातक मोह नामका विकार है। मोह अर्थात् विपरीताभिनिवेश या मिथ्यात्वसे अन्य सभी विकार बलवान बनते हैं मोहके हट जाने पर अन्य विकार धीरे धीरे निष्प्राण हो जाते हैं। न्यायवैशेषिकोंका मिथ्याज्ञान, सांख्य योगोंका विवेकाज्ञान, बौद्धोंकी अविद्या या सत्त्वदृष्टि, इसी मोहके नामान्तर हैं। बन्धके कारणोंमें इसीकी प्रधानता है इसके बिना अन्य बन्धके कारण अपनी उत्कृष्ट स्थिति या तीव्रतम अनुभागसे कर्मों को नहीं बाँध सकते ।
न्यायसूत्रमें दोषोंकी वे ही तीन जातियाँ बताई हैं जो श्रा० कुन्दकुन्दने प्रवचनसार (११८४) में निर्दिष्ट की हैं। न्यायसूत्रमें इन तीन राशियोंमें मोहको सबसे तीव्र पापबन्धक कहा है। जैन कार्मिकपरम्परामें मोहका कर्मों के सेनापति रूपसे वर्णन मिलता है। इस सेनानायकके बलपर ही समस्त सेनामें जोश और कार्यक्षमता बनी रहती है। इसके अभावमें धीरे धीरे अन्य कर्म निर्बल हो जाते हैं।
मोहनीय कर्मके दो भेद हैं-एक दर्शनमोहनीय और दूसरा चारित्र मोहनीय। इनमें मोहनीयका दर्शन मोहनीय भेद राग, द्वेष, मोहकी त्रिपुटीमें मोहशब्दका वाच्य होता है। स्वामी समन्तभद्रने दर्शनमोही साधुसे निर्मोही गृहस्थको कल्याणमार्गका पथिक तथा उत्कृष्ट बताया है। दूसरा चारित्रमोहनीय भेद मूलतः कषाय और नोकषायोंमें विभाजित होता है। ये कषायें राग द्वेषमें विभाजित होकर एक मोहनीय कर्मको 'राग द्वेष मोह' इस त्रिरूपताका बाना पहिना देती हैं।
(१) "तत्त्रैराश्यं रागद्वेषमोहानर्थान्तरभावात् । तेषां मोहः पापीयानामूढस्येतरोत्पत्तेः ।"-न्यायसू० ४।१।३,६।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org