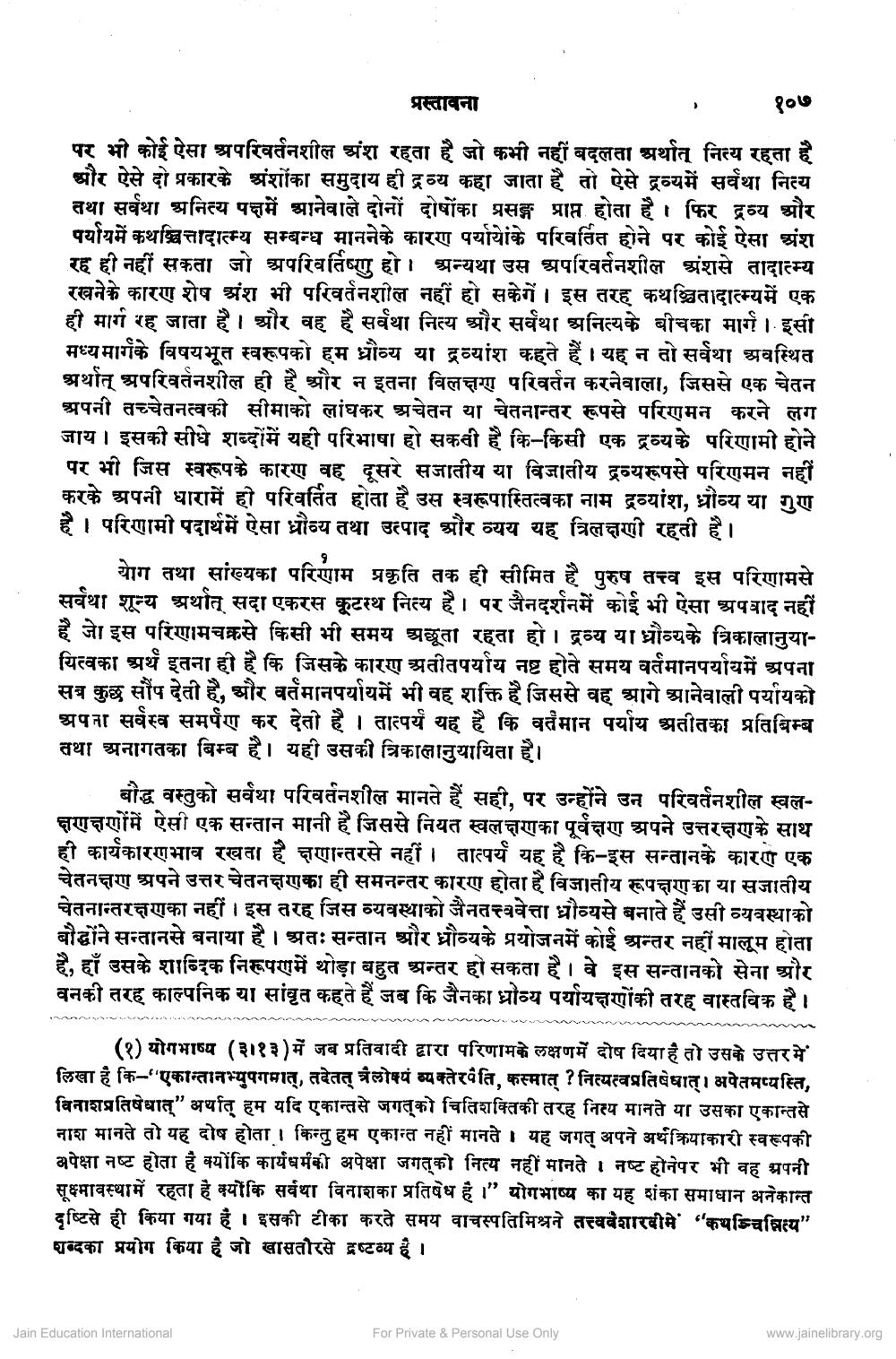________________
प्रस्तावना
१०७
पर भी कोई ऐसा अपरिवर्तनशील अंश रहता है जो कभी नहीं बदलता अर्थात् नित्य रहता है
और ऐसे दो प्रकारके अंशोंका समुदाय ही द्रव्य कहा जाता है तो ऐसे द्रव्यमें सर्वथा नित्य तथा सर्वथा अनित्य पक्षमें आनेवाले दोनों दोषोंका प्रसङ्ग प्राप्त होता है। फिर द्रव्य और पर्यायमें कथञ्चित्तादात्म्य सम्बन्ध माननेके कारण पर्यायोंके परिवर्तित होने पर कोई ऐसा अंश रह ही नहीं सकता जो अपरिवर्तिष्णु हो। अन्यथा उस अपरिवर्तनशील अंशसे तादात्म्य रखनेके कारण शेष अंश भी परिवर्तनशील नहीं हो सकेगें। इस तरह कथञ्चितादात्म्यमें एक ही मार्ग रह जाता है। और वह है सर्वथा नित्य और सर्वथा अनित्यके बीचका मार्ग। इसी मध्यमार्गके विषयभूत स्वरूपको हम ध्रौव्य या द्रव्यांश कहते हैं । यह न तो सर्वथा अवस्थित अर्थात् अपरिवर्तनशील ही है और न इतना विलक्षण परिवर्तन करनेवाला, जिससे एक चेतन अपनी तच्चेतनत्वको सीमाको लांघकर अचेतन या चेतनान्तर रूपसे परिणमन करने लग जाय। इसकी सीधे शब्दोंमें यही परिभाषा हो सकती है कि-किसी एक द्रव्य के परिणामी होने पर भी जिस स्वरूपके कारण वह दूसरे सजातीय या विजातीय द्रव्यरूपसे परिणमन नहीं करके अपनी धारामें हो परिवर्तित होता है उस स्वरूपास्तित्वका नाम द्रव्यांश, ध्रौव्य या गुण है । परिणामी पदार्थमें ऐसा ध्रौव्य तथा उत्पाद और व्यय यह त्रिलक्षणी रहती है।
योग तथा सांख्यका परिणाम प्रकृति तक ही सीमित है पुरुष तत्त्व इस परिणामसे सर्वथा शून्य अर्थात् सदा एकरस कूटस्थ नित्य है। पर जैनदर्शनमें कोई भी ऐसा अपवाद नहीं है जो इस परिणामचक्रसे किसी भी समय अछूता रहता हो। द्रव्य या ध्रौव्यके त्रिकालानुयायित्वका अर्थ इतना ही है कि जिसके कारण अतीतपर्याय नष्ट होते समय वर्तमानपर्यायमें अपना सब कुछ सौंप देती है, और वर्तमानपर्यायमें भी वह शक्ति है जिससे वह आगे आनेवाली पर्यायको अपना सर्वस्व समर्पण कर देती है । तात्पर्य यह है कि वर्तमान पर्याय अतीतका प्रतिबिम्ब तथा अनागतका बिम्ब है। यही उसकी त्रिकालानुयायिता है।
बौद्ध वस्तुको सर्वथा परिवर्तनशील मानते हैं सही, पर उन्होंने उन परिवर्तनशील स्वलक्षणक्षणों में ऐसी एक सन्तान मानी है जिससे नियत स्वलक्षणका पूर्वक्षण अपने उत्तरक्षणके साथ ही कार्यकारणभाव रखता है क्षणान्तरसे नहीं। तात्पर्य यह है कि इस सन्तानके कारण एक चेतनक्षण अपने उत्तर चेतनक्षणका ही समनन्तर कारण होता है विजातीय रूपक्षणका या सजातीय चेतनान्तरक्षणका नहीं। इस तरह जिस व्यवस्थाको जैनतत्त्ववेत्ता ध्रौव्यसे बनाते हैं उसी व्यवस्थाको बौद्धोंने सन्तानसे बनाया है। अतः सन्तान और ध्रौव्यके प्रयोजनमें कोई अन्तर नहीं मालूम होता है, हाँ उसके शाब्दिक निरूपणमें थोड़ा बहुत अन्तर हो सकता है। वे इस सन्तानको सेना और वनकी तरह काल्पनिक या सांवृत कहते हैं जब कि जैनका ध्रोव्य पर्यायक्षणोंकी तरह वास्तविक है।
(१) योगभाष्य (३।१३) में जब प्रतिवादी द्वारा परिणामके लक्षणमें दोष दिया है तो उसके उत्तर में लिखा है कि-"एकान्तानभ्युपगमात्, तदेतत् त्रैलोक्यं व्यक्तेरपति, कस्मात् ? नित्यत्वप्रतिषेधात्। अपेतमप्यस्ति, विनाशप्रतिषेधात्" अर्थात् हम यदि एकान्तसे जगत्को चितिशक्तिकी तरह नित्य मानते या उसका एकान्तसे नाश मानते तो यह दोष होता। किन्तु हम एकान्त नहीं मानते। यह जगत् अपने अर्थक्रियाकारी स्वरूपकी अपेक्षा नष्ट होता है क्योंकि कार्यधर्मकी अपेक्षा जगत्को नित्य नहीं मानते । नष्ट होनेपर भी वह अपनी सूक्ष्मावस्थामें रहता है क्योंकि सर्वथा विनाशका प्रतिषेध है ।" योगभाष्य का यह शंका समाधान अनेकान्त दृष्टिसे ही किया गया है । इसकी टीका करते समय वाचस्पतिमिश्रने तत्त्ववेशारदीमें "कथञ्चिन्नित्य" शब्दका प्रयोग किया है जो खासतौरसे द्रष्टव्य है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org