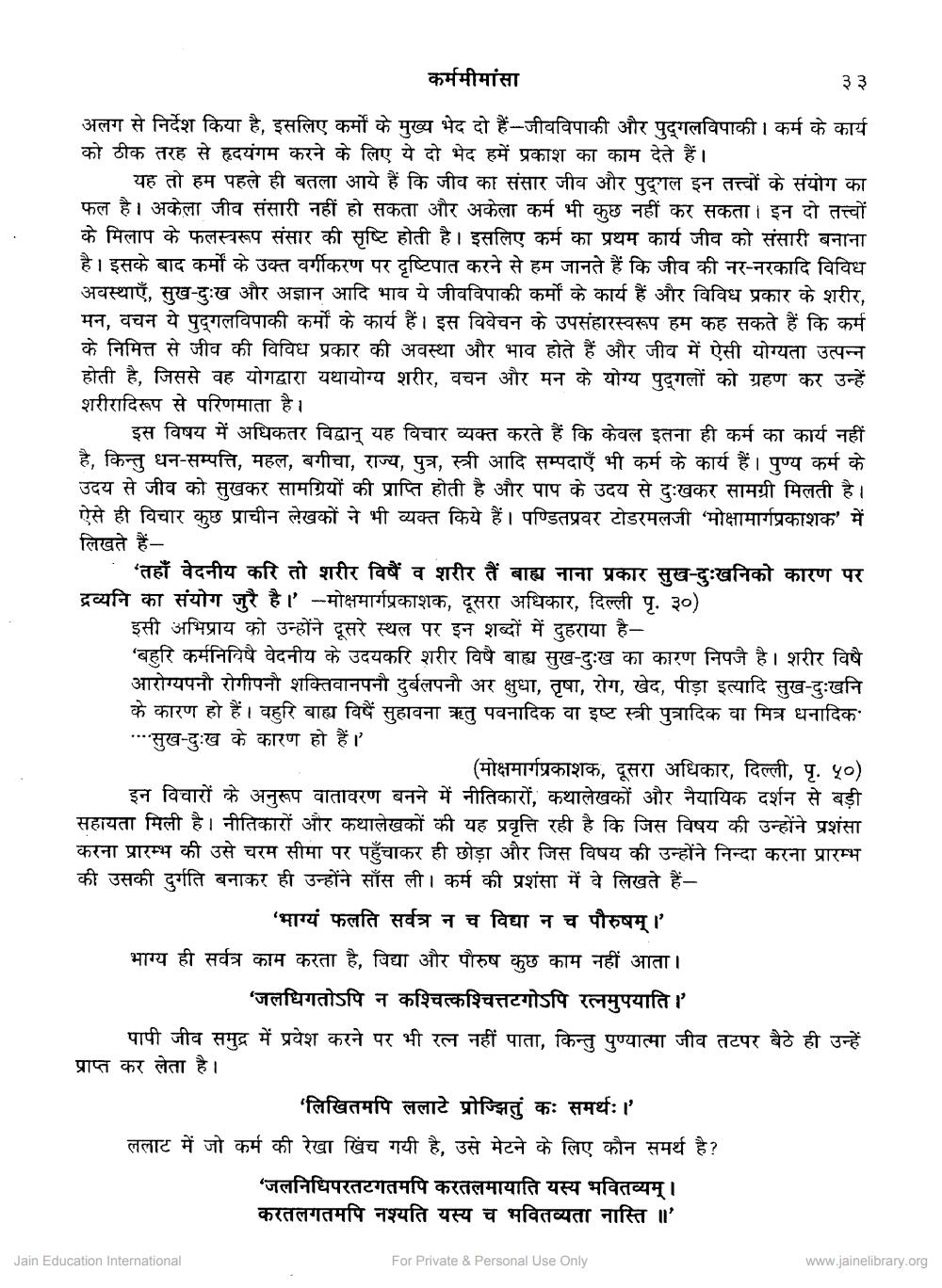________________
कर्ममीमांसा
३३
अलग से निर्देश किया है, इसलिए कर्मों के मुख्य भेद दो हैं-जीवविपाकी और पुद्गलविपाकी। कर्म के कार्य को ठीक तरह से हृदयंगम करने के लिए ये दो भेद हमें प्रकाश का काम देते हैं।
यह तो हम पहले ही बतला आये हैं कि जीव का संसार जीव और पुद्गल इन तत्त्वों के संयोग का फल है। अकेला जीव संसारी नहीं हो सकता और अकेला कर्म भी कुछ नहीं कर सकता। इन दो तत्त्वों के मिलाप के फलस्वरूप संसार की सृष्टि होती है। इसलिए कर्म का प्रथम कार्य जीव को संसारी बनाना है। इसके बाद कर्मों के उक्त वर्गीकरण पर दृष्टिपात करने से हम जानते हैं कि जीव की नर-नरकादि विविध अवस्थाएँ, सुख-दुःख और अज्ञान आदि भाव ये जीवविपाकी कर्मों के कार्य हैं और विविध प्रकार के शरीर, मन, वचन ये पुद्गलविपाकी कर्मों के कार्य हैं। इस विवेचन के उपसंहारस्वरूप हम कह सकते हैं कि कर्म के निमित्त से जीव की विविध प्रकार की अवस्था और भाव होते हैं और जीव में ऐसी योग्यता उत्पन्न होती है, जिससे वह योगद्वारा यथायोग्य शरीर, वचन और मन के योग्य पुद्गलों को ग्रहण कर उन्हें शरीरादिरूप से परिणमाता है।
इस विषय में अधिकतर विद्वान् यह विचार व्यक्त करते हैं कि केवल इतना ही कर्म का कार्य नहीं है, किन्तु धन-सम्पत्ति, महल, बगीचा, राज्य, पुत्र, स्त्री आदि सम्पदाएँ भी कर्म के कार्य हैं। पुण्य कर्म के उदय से जीव को सखकर सामग्रियों की प्राप्ति होती है और पाप के उदय से दःखकर सामग्री मिलत ऐसे ही विचार कुछ प्राचीन लेखकों ने भी व्यक्त किये हैं। पण्डितप्रवर टोडरमलजी 'मोक्षामार्गप्रकाशक' में लिखते हैं
- 'तहाँ वेदनीय करि तो शरीर विर्षे व शरीर तैं बाह्य नाना प्रकार सुख-दुःखनिको कारण पर द्रव्यनि का संयोग जुरै है।' -मोक्षमार्गप्रकाशक, दूसरा अधिकार, दिल्ली पृ. ३०)
इसी अभिप्राय को उन्होंने दूसरे स्थल पर इन शब्दों में दुहराया है'बहरि कर्मनिविषै वेदनीय के उदयकरि शरीर विषै बाह्य सुख-दुःख का कारण निपजै है। शरीर विषै आरोग्यपनौ रोगीपनौ शक्तिवानपनौ दुर्बलपनौ अर क्षधा, तषा, रोग, खेद, पीडा इत्यादि सख-दःखनि के कारण हो हैं। वहुरि बाह्य विर्षे सुहावना ऋतु पवनादिक वा इष्ट स्त्री पुत्रादिक वा मित्र धनादिक .. सुख-दुःख के कारण हो हैं।'
(मोक्षमार्गप्रकाशक, दूसरा अधिकार, दिल्ली, पृ. ५०) इन विचारों के अनुरूप वातावरण बनने में नीतिकारों, कथालेखकों और नैयायिक दर्शन से बड़ी सहायता मिली है। नीतिकारों और कथालेखकों की यह प्रवृत्ति रही है कि जिस विषय की उन्होंने प्रशंसा
म्भ की उसे चरम सीमा पर पहुँचाकर ही छोड़ा और जिस विषय की उन्होंने निन्दा करना प्रारम्भ की उसकी दुर्गति बनाकर ही उन्होंने साँस ली। कर्म की प्रशंसा में वे लिखते हैं
_ 'भाग्यं फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम्।' भाग्य ही सर्वत्र काम करता है, विद्या और पौरुष कुछ काम नहीं आता।
'जलधिगतोऽपि न कश्चित्कश्चित्तटगोऽपि रत्नमुपयाति।' पापी जीव समुद्र में प्रवेश करने पर भी रत्न नहीं पाता, किन्तु पुण्यात्मा जीव तटपर बैठे ही उन्हें प्राप्त कर लेता है।
'लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितुं कः समर्थः।' ललाट में जो कर्म की रेखा खिंच गयी है, उसे मेटने के लिए कौन समर्थ है?
'जलनिधिपरतटगतमपि करतलमायाति यस्य भवितव्यम्। करतलगतमपि नश्यति यस्य च भवितव्यता नास्ति ॥'
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org