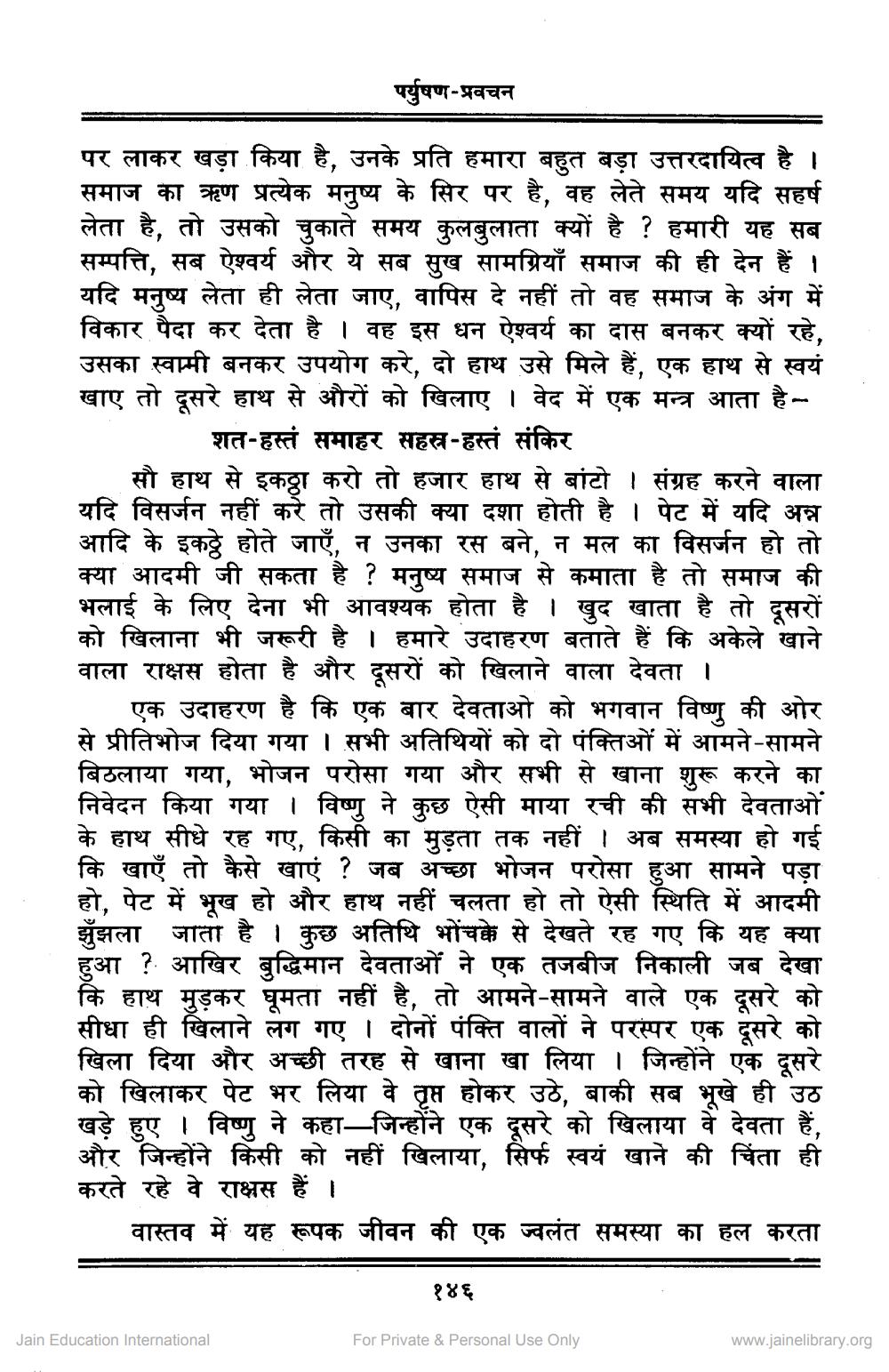________________
पर्युषण-प्रवचन
पर लाकर खड़ा किया है, उनके प्रति हमारा बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है । समाज का ऋण प्रत्येक मनुष्य के सिर पर है, वह लेते समय यदि सहर्ष लेता है, तो उसको चुकाते समय कुलबुलाता क्यों है ? हमारी यह सब सम्पत्ति, सब ऐश्वर्य और ये सब सुख सामग्रियाँ समाज की ही देन हैं । यदि मनुष्य लेता ही लेता जाए, वापिस दे नहीं तो वह समाज के अंग में विकार पैदा कर देता है । वह इस धन ऐश्वर्य का दास बनकर क्यों रहे, उसका स्वामी बनकर उपयोग करे, दो हाथ उसे मिले हैं, एक हाथ से स्वयं खाए तो दूसरे हाथ से औरों को खिलाए । वेद में एक मन्त्र आता है
शत- हस्तं समाहर सहस्र - हस्तं संकिर
सौ हाथ से इकठ्ठा करो तो हजार हाथ से बांटो । संग्रह करने वाला यदि विसर्जन नहीं करे तो उसकी क्या दशा होती है । पेट में यदि अन्न आदि के इकठ्ठे होते जाएँ, न उनका रस बने, न मल का विसर्जन हो तो क्या आदमी जी सकता है ? मनुष्य समाज से कमाता है तो समाज की भलाई के लिए देना भी आवश्यक होता है । खुद खाता है तो दूसरों को खिलाना भी जरूरी है । हमारे उदाहरण बताते हैं कि अकेले खाने वाला राक्षस होता है और दूसरों को खिलाने वाला देवता ।
एक उदाहरण है कि एक बार देवताओ को भगवान विष्णु की ओर से प्रीतिभोज दिया गया । सभी अतिथियों को दो पंक्तिओं में आमने-सामने बिठलाया गया, भोजन परोसा गया और सभी से खाना शुरू करने का निवेदन किया गया । विष्णु ने कुछ ऐसी माया रची की सभी देवताओं के हाथ सीधे रह गए, किसी का मुड़ता तक नहीं । अब समस्या हो गई कि खाएँ तो कैसे खाएं ? जब अच्छा भोजन परोसा हुआ सामने पड़ा हो, पेट में भूख हो और हाथ नहीं चलता हो तो ऐसी स्थिति में आदमी झुंझला जाता है कुछ अतिथि भोचक्के से देखते रह गए कि यह क्या हुआ ? आखिर बुद्धिमान देवताओं ने एक तजबीज निकाली जब देखा कि हाथ मुड़कर घूमता नहीं है, तो आमने-सामने वाले एक दूसरे को सीधा ही खिलाने लग गए । दोनों पंक्ति वालों ने परस्पर एक दूसरे को खिला दिया और अच्छी तरह से खाना खा लिया जिन्होंने एक दूसरे को खिलाकर पेट भर लिया वे तृप्त होकर उठे, बाकी सब भूखे ही उठ खड़े हुए । विष्णु ने कहा- जिन्होंने एक दूसरे को खिलाया वे देवता हैं, और जिन्होंने किसी को नहीं खिलाया, सिर्फ स्वयं खाने की चिंता ही करते रहे वे राक्षस हैं ।
वास्तव में यह रूपक जीवन की एक ज्वलंत समस्या का हल करता
Jain Education International
१४६
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org