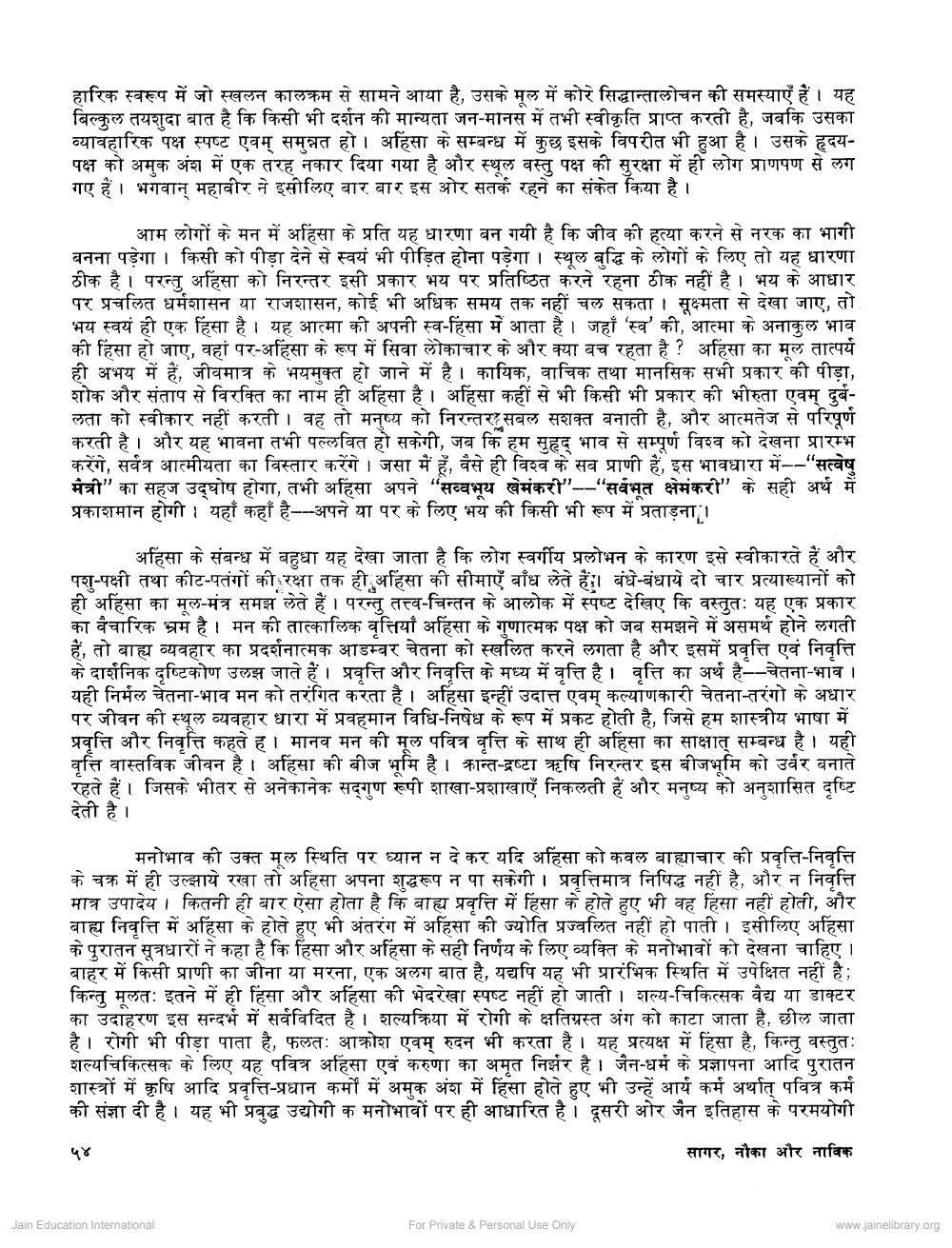________________
हारिक स्वरूप में जो स्खलन कालक्रम से सामने आया है, उसके मूल में कोरे सिद्धान्तालोचन की समस्याएँ हैं। यह बिल्कुल तयशुदा बात है कि किसी भी दर्शन की मान्यता जन-मानस में तभी स्वीकृति प्राप्त करती है, जबकि उसका व्यावहारिक पक्ष स्पष्ट एवम् समुन्नत हो अहिंसा के सम्बन्ध में कुछ इसके विपरीत भी हुआ है। उसके हृदयपक्ष को अमुक अंश में एक तरह नकार दिया गया है और स्थूल वस्तु पक्ष की सुरक्षा में ही लोग प्राणपण से लग गए हैं । भगवान् महावीर ने इसीलिए बार बार इस ओर सतर्क रहने का संकेत किया है ।
आम लोगों के मन में अहिंसा के प्रति यह धारणा बन गयी है कि जीव की हत्या करने से नरक का भागी बनना पड़ेगा। किसी को पीड़ा देने से स्वयं भी पीड़ित होना पड़ेगा। स्थूल बुद्धि के लोगों के लिए तो यह धारणा ठीक है परन्तु अहिंसा को निरन्तर इसी प्रकार भय पर प्रतिष्ठित करने रहना ठीक नहीं है। भय के आधार पर प्रचलित धर्मशासन या राजशासन, कोई भी अधिक समय तक नहीं चल सकता। सूक्ष्मता से देखा जाए, तो भय स्वयं ही एक हिंसा है। यह आत्मा की अपनी स्व-हिंसा में आता है। जहाँ 'स्व' की, आत्मा के अनाकुल भाव की हिंसा हो जाए, वहां पर अहिंसा के रूप में सिवा लोकाचार के और क्या बच रहता है ? अहिंसा का मूल तात्पर्य ही अभय में हैं, जीवमात्र के भयमुक्त हो जाने में है। कायिक, वाचिक तथा मानसिक सभी प्रकार की पीड़ा, शोक और संताप से विरक्ति का नाम ही अहिंसा है । अहिंसा कहीं से भी किसी भी प्रकार की भीरुता एवम् दुर्बलता को स्वीकार नहीं करती। वह तो मनुष्य को निरन्तर सबल सशक्त बनाती है, और आत्मतेज से परिपूर्ण करती है । और यह भावना तभी पल्लवित हो सकेगी, जब कि हम सुहृद् भाव से सम्पूर्ण विश्व को देखना प्रारम्भ करेंगे, सर्वत्र आत्मीयता का विस्तार करेंगे । जसा में हूँ, वैसे ही विश्व के सब प्राणी हैं, इस भावधारा में -- "सत्वेषु मंत्री" का सहज उद्घोष होगा, तभी अहिंसा अपने " सव्वभूय खेमंकरी" - "सर्वभूत क्षेमंकरी" के सही अर्थ मैं प्रकाशमान होगी । यहाँ कहाँ है --- अपने या पर के लिए भय की किसी भी रूप में प्रताड़ना ।
अहिंसा के संबन्ध में बहुधा यह देखा जाता है कि लोग स्वर्गीय प्रलोभन के कारण इसे स्वीकारते हैं और पशु-पक्षी तथा कीट-पतंगों की रक्षा तक ही अहिंसा की सीमाएँ बाँध लेते हैं। बंधे-बंधायें दो चार प्रत्याख्यानों को ही अहिंसा का मूल-मंत्र समझ लेते हैं । परन्तु तत्त्व - चिन्तन के आलोक में स्पष्ट देखिए कि वस्तुतः यह एक प्रकार का वैचारिक भ्रम है । मन की तात्कालिक वृत्तियाँ अहिंसा के गुणात्मक पक्ष को जब समझने में असमर्थ होने लगती हैं, तो बाह्य व्यवहार का प्रदर्शनात्मक आडम्बर चेतना को स्खलित करने लगता है और इसमें प्रवृत्ति एवं निवृत्ति के दार्शनिक दृष्टिकोण उलझ जाते हैं । प्रवृत्ति और निवृत्ति के मध्य में वृत्ति है । वृत्ति का अर्थ है -- चेतना - भाव । यही निर्मल चेतना-भाव मन को तरंगित करता है । अहिंसा इन्हीं उदात्त एवम् कल्याणकारी चेतना-तरंगो के अधार पर जीवन की स्थूल व्यवहार धारा में प्रवहमान विधि-निषेध के रूप में प्रकट होती है, जिसे हम शास्त्रीय भाषा में प्रवृत्ति और निवृत्ति कहते है। मानव मन की मूल पवित्र वृत्ति के साथ ही अहिंसा का साक्षात् सम्बन्ध है। यही वृत्ति वास्तविक जीवन है। अहिंसा की बीज भूमि है। कान्त द्रष्टा ऋषि निरन्तर इस बीजभूमि को उर्वर बनाते रहते हैं। जिसके भीतर से अनेकानेक सद्गुण रूपी शाखा प्रशाखाएँ निकलती हैं और मनुष्य को अनुशासित दृष्टि देती है।
मनोभाव की उक्त मूल स्थिति पर ध्यान न दे कर यदि अहिंसा को कवल बाह्याचार की प्रवृत्ति निवृत्ति के चक्र में ही उल्झाये रखा तो अहिसा अपना शुद्धरूप न पा सकेगी। प्रवृत्तिमात्र निषिद्ध नहीं है, और न निवृत्ति मात्र उपादेय। कितनी ही बार ऐसा होता है कि बाह्य प्रवृत्ति में हिंसा के होते हुए भी वह हिंसा नहीं होती, और बाह्य निवृत्ति में अहिंसा के होते हुए भी अंतरंग में अहिंसा की ज्योति प्रज्वलित नहीं हो पाती। इसीलिए अहिंसा के पुरातन सूत्रधारों ने कहा है कि हिंसा और अहिंसा के सही निर्णय के लिए व्यक्ति के मनोभावों को देखना चाहिए। बाहर में किसी प्राणी का जीना या मरना एक अलग बात है, यद्यपि यह भी प्रारंभिक स्थिति में उपेक्षित नहीं है। किन्तु मूलतः इतने में ही हिंसा और अहिंसा की भेदरेखा स्पष्ट नहीं हो जाती। शल्य चिकित्सक वैद्य या डॉक्टर का उदाहरण इस सन्दर्भ में सर्वविदित है। शल्यक्रिया में रोगी के क्षतिग्रस्त अंग को काटा जाता है, छील जाता है। रोगी भी पीड़ा पाता है, फलतः आक्रोश एवम् रुदन भी करता है। यह प्रत्यक्ष में हिंसा है, किन्तु वस्तुतः शल्यचिकित्सक के लिए यह पवित्र अहिंसा एवं करुणा का अमृत निर्झर है। जैन धर्म के प्रज्ञापना आदि पुरातन शास्त्रों में कृषि आदि प्रवृत्ति प्रधान कर्मों में अमुक अंश में हिंसा होते हुए भी उन्हें आयें कर्म अर्थात् पवित्र कर्म की संज्ञा दी है । यह भी प्रबुद्ध उद्योगी क मनोभावों पर ही आधारित है । दूसरी ओर जैन इतिहास के परमयोगी
५४
सागर, नौका और नाविक
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org.