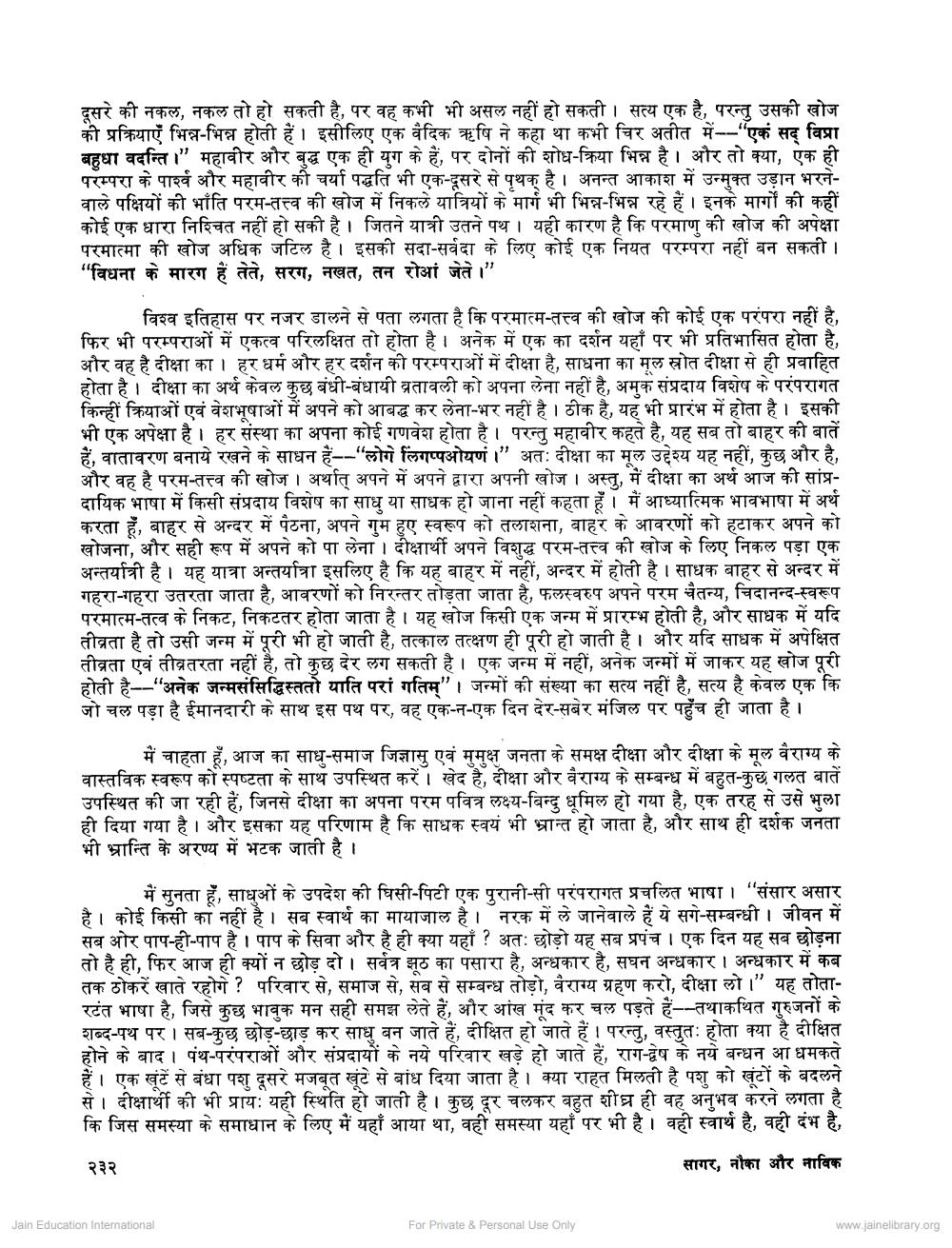________________
दूसरे की नकल, नकल तो हो सकती है, पर वह कभी भी असल नहीं हो सकती। सत्य एक है, परन्तु उसकी खोज की प्रक्रियाएँ भिन्न-भिन्न होती हैं। इसीलिए एक वैदिक ऋषि ने कहा था कभी चिर अतीत में--"एक सद् विप्रा बहुधा वदन्ति ।" महावीर और बुद्ध एक ही युग के हैं, पर दोनों की शोध-क्रिया भिन्न है। और तो क्या, एक ही परम्परा के पार्श्व और महावीर की चर्या पद्धति भी एक-दूसरे से पृथक् है। अनन्त आकाश में उन्मुक्त उड़ान भरनेवाले पक्षियों की भाँति परम-तत्त्व की खोज में निकले यात्रियों के मार्ग भी भिन्न-भिन्न रहे हैं। इनके मार्गों की कहीं कोई एक धारा निश्चित नहीं हो सकी है। जितने यात्री उतने पथ। यही कारण है कि परमाणु की खोज की अपेक्षा परमात्मा की खोज अधिक जटिल है। इसकी सदा-सर्वदा के लिए कोई एक नियत परम्परा नहीं बन सकती। "विधना के मारग हैं तेते, सरग, नखत, तन रोआं जेते।"
विश्व इतिहास पर नजर डालने से पता लगता है कि परमात्म-तत्त्व की खोज की कोई एक परंपरा नहीं है, फिर भी परम्पराओं में एकत्व परिलक्षित तो होता है। अनेक में एक का दर्शन यहाँ पर भी प्रतिभासित होता है,
और वह है दीक्षा का। हर धर्म और हर दर्शन की परम्पराओं में दीक्षा है, साधना का मल स्रोत दीक्षा से ही प्रवाहित होता है। दीक्षा का अर्थ केवल कुछ बंधी-बंधायी व्रतावली को अपना लेना नहीं है, अमक संप्रदाय विशेष के परंपरागत किन्हीं क्रियाओं एवं वेशभूषाओं में अपने को आबद्ध कर लेना-भर नहीं है। ठीक है, यह भी प्रारंभ में होता है। इसकी भी एक अपेक्षा है। हर संस्था का अपना कोई गणवेश होता है। परन्तु महावीर कहते है, यह सब तो बाहर की बातें हैं, वातावरण बनाये रखने के साधन हैं--"लोगे लिंगप्पओयणं।" अत: दीक्षा का मूल उद्देश्य यह नहीं, कुछ और है, और वह है परम-तत्त्व की खोज । अर्थात् अपने में अपने द्वारा अपनी खोज । अस्तु, मैं दीक्षा का अर्थ आज की सांप्रदायिक भाषा में किसी संप्रदाय विशेष का साधु या साधक हो जाना नहीं कहता हूँ। मैं आध्यात्मिक भावभाषा में अर्थ करता हूँ, बाहर से अन्दर में पैठना, अपने गुम हुए स्वरूप को तलाशना, बाहर के आवरणों को हटाकर अपने को खोजना, और सही रूप में अपने को पा लेना। दीक्षार्थी अपने विशुद्ध परम-तत्त्व की खोज के लिए निकल पड़ा एक अन्तर्यात्री है। यह यात्रा अन्तर्यात्रा इसलिए है कि यह बाहर में नहीं, अन्दर में होती है। साधक बाहर से अन्दर में गहरा-गहरा उतरता जाता है, आवरणों को निरन्तर तोड़ता जाता है, फलस्वरुप अपने परम चैतन्य, चिदानन्द-स्वरूप परमात्म-तत्व के निकट, निकटतर होता जाता है। यह खोज किसी एक जन्म में प्रारम्भ होती है, और साधक में यदि तीव्रता है तो उसी जन्म में पूरी भी हो जाती है, तत्काल तत्क्षण ही पूरी हो जाती है। और यदि साधक में अपेक्षित तीव्रता एवं तीव्रतरता नहीं है, तो कुछ देर लग सकती है। एक जन्म में नहीं, अनेक जन्मों में जाकर यह खोज पूरी होती है-"अनेक जन्मसंसिद्धिस्ततो याति परां गतिम्” । जन्मों की संख्या का सत्य नहीं है, सत्य है केवल एक कि जो चल पड़ा है ईमानदारी के साथ इस पथ पर, वह एक-न-एक दिन देर-सबेर मंजिल पर पहुँच ही जाता है।
में चाहता हूँ, आज का साधु-समाज जिज्ञासु एवं मुमुक्ष जनता के समक्ष दीक्षा और दीक्षा के मल वैराग्य के वास्तविक स्वरूप को स्पष्टता के साथ उपस्थित करें। खेद है, दीक्षा और वैराग्य के सम्बन्ध में बहुत-कुछ गलत बातें उपस्थित की जा रही हैं, जिनसे दीक्षा का अपना परम पवित्र लक्ष्य-बिन्दु धूमिल हो गया है, एक तरह से उसे भुला ही दिया गया है। और इसका यह परिणाम है कि साधक स्वयं भी भ्रान्त हो जाता है, और साथ ही दर्शक जनता भी भ्रान्ति के अरण्य में भटक जाती है।
मैं सुनता हूँ, साधुओं के उपदेश की घिसी-पिटी एक पुरानी-सी परंपरागत प्रचलित भाषा। "संसार असार है। कोई किसी का नहीं है। सब स्वार्थ का मायाजाल है। नरक में ले जानेवाले हैं ये सगे-सम्बन्धी। जीवन में सब ओर पाप-ही-पाप है। पाप के सिवा और है ही क्या यहाँ ? अतः छोड़ो यह सब प्रपंच । एक दिन यह सब छोड़ना तो है ही, फिर आज ही क्यों न छोड़ दो। सर्वत्र झूठ का पसारा है, अन्धकार है, सघन अन्धकार । अन्धकार में कब तक ठोकरें खाते रहोगे? परिवार से, समाज से, सब से सम्बन्ध तोड़ो, वैराग्य ग्रहण करो, दीक्षा लो।" यह तोतारटंत भाषा है, जिसे कुछ भावुक मन सही समझ लेते हैं, और आंख मूंद कर चल पड़ते हैं--तथाकथित गुरुजनों के शब्द-पथ पर । सब-कुछ छोड़-छाड़ कर साधु बन जाते हैं, दीक्षित हो जाते हैं । परन्तु, वस्तुतः होता क्या है दीक्षित होने के बाद। पंथ-परंपराओं और संप्रदायों के नये परिवार खड़े हो जाते हैं, राग-द्वेष के नये बन्धन आ धमकते हैं। एक खूटे से बंधा पशु दूसरे मजबूत खूटे से बांध दिया जाता है। क्या राहत मिलती है पशु को खूटों के बदलने से। दीक्षार्थी की भी प्रायः यही स्थिति हो जाती है। कुछ दूर चलकर बहुत शीघ्र ही वह अनुभव करने लगता है कि जिस समस्या के समाधान के लिए मैं यहाँ आया था, वही समस्या यहाँ पर भी है। वही स्वार्थ है, वही दंभ है,
२३२
सागर, नौका और नाविक
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org