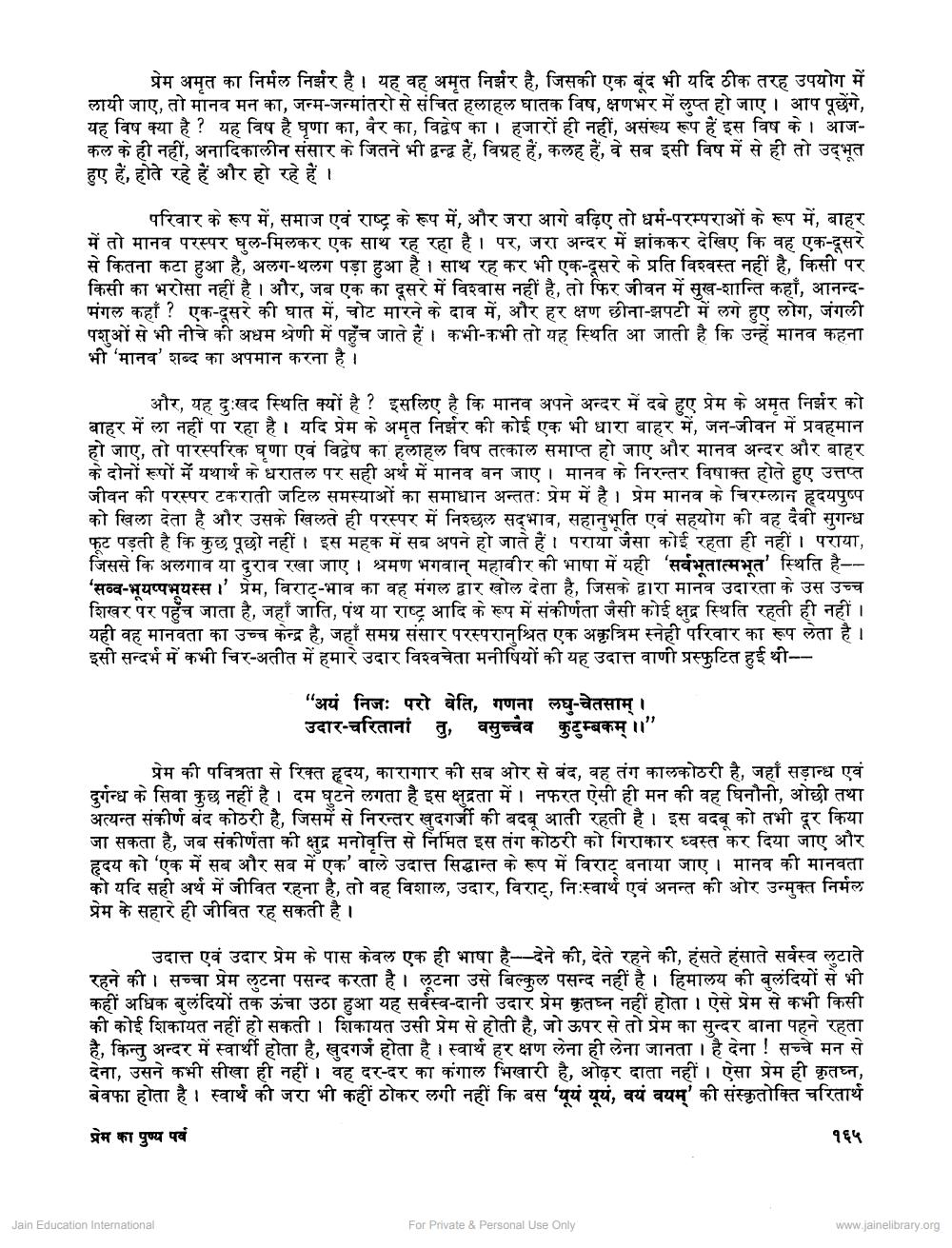________________
प्रेम अमृत का निर्मल निर्झर है। यह वह अमृत निर्झर है, जिसकी एक बूंद भी यदि ठीक तरह उपयोग में लायी जाए, तो मानव मन का, जन्म-जन्मांतरो से संचित हलाहल घातक विष, क्षणभर में लुप्त हो जाए। आप पूछेगे, यह विष क्या है ? यह विष है घृणा का, वैर का, विद्वेष का। हजारों ही नहीं, असंख्य रूप हैं इस विष के। आजकल के ही नहीं, अनादिकालीन संसार के जितने भी द्वन्द्व हैं, विग्रह हैं, कलह हैं, वे सब इसी विष में से ही तो उद्भुत हुए हैं, होते रहे हैं और हो रहे हैं ।
परिवार के रूप में, समाज एवं राष्ट्र के रूप में, और जरा आगे बढ़िए तो धर्म-परम्पराओं के रूप में, बाहर में तो मानव परस्पर घुल-मिलकर एक साथ रह रहा है। पर, जरा अन्दर में झांककर देखिए कि वह एक-दूसरे से कितना कटा हुआ है, अलग-थलग पड़ा हुआ है। साथ रह कर भी एक-दूसरे के प्रति विश्वस्त नहीं है, किसी पर किसी का भरोसा नहीं है। और, जब एक का दूसरे में विश्वास नहीं है, तो फिर जीवन में सुख-शान्ति कहाँ, आनन्दमंगल कहाँ ? एक-दूसरे की घात में, चोट मारने के दाव में, और हर क्षण छीना-झपटी में लगे हुए लोग, जंगली पशुओं से भी नीचे की अधम श्रेणी में पहुँच जाते हैं। कभी-कभी तो यह स्थिति आ जाती है कि उन्हें मानव कहना भी 'मानव' शब्द का अपमान करना है।
समस्याओं का समाधान सदभाव, सहानुभूति कोई रहता ही
और, यह दुःखद स्थिति क्यों है ? इसलिए है कि मानव अपने अन्दर में दबे हए प्रेम के अमत निर्झर को बाहर में ला नहीं पा रहा है। यदि प्रेम के अमृत निर्झर की कोई एक भी धारा बाहर में, जन-जीवन में प्रवहमान हो जाए, तो पारस्परिक घृणा एवं विद्वेष का हलाहल विष तत्काल समाप्त हो जाए और मानव अन्दर और बाहर के दोनों रूपों में यथार्थ के धरातल पर सही अर्थ में मानव बन जाए। मानव के निरन्तर विषाक्त होते हुए उत्तप्त जीवन की परस्पर टकराती जटिल समस्याओं का समाधान अन्ततः प्रेम में है। प्रेम मानव के चिरम्लान हृदयपुष्प को खिला देता है और उसके खिलते ही परस्पर में निश्छल सदभाव, सहानभति एवं सहयोग की वह दैवी सुगन्ध फूट पड़ती है कि कुछ पूछो नहीं। इस महक में सब अपने हो जाते हैं। पराया जैसा कोई रहता ही नहीं। पराया, जिससे कि अलगाव या दुराव रखा जाए। श्रमण भगवान् महावीर की भाषा में यही 'सर्वभूतात्मभूत' स्थिति है-- 'सव्व-भूयप्पभूयस्स।' प्रेम, विराट-भाव का वह मंगल द्वार खोल देता है, जिसके द्वारा मानव उदारता के उस उच्च शिखर पर पहुँच जाता है, जहाँ जाति, पंथ या राष्ट्र आदि के रूप में संकीर्णता जैसी कोई क्षुद्र स्थिति रहती ही नहीं। यही वह मानवता का उच्च केन्द्र है, जहाँ समग्र संसार परस्परानुश्रित एक अकृत्रिम स्नेही परिवार का रूप लेता है। इसी सन्दर्भ में कभी चिर-अतीत में हमारे उदार विश्वचेता मनीषियों की यह उदात्त वाणी प्रस्फुटित हुई थी--
"अयं निजः परो वेति, गणना लघु-चेतसाम् । उदार-चरितानां तु, वसुच्चैव कुटुम्बकम् ॥"
प्रेम की पवित्रता से रिक्त हृदय, कारागार की सब ओर से बंद, वह तंग कालकोठरी है, जहाँ सड़ान्ध एवं दुर्गन्ध के सिवा कुछ नहीं है। दम घुटने लगता है इस क्षुद्रता में। नफरत ऐसी ही मन की वह घिनौनी, ओछी तथा अत्यन्त संकीर्ण बंद कोठरी है, जिसमें से निरन्तर खुदगर्जी की बदबू आती रहती है। इस बदबू को तभी दूर किया जा सकता है, जब संकीर्णता की क्षुद्र मनोवृत्ति से निर्मित इस तंग कोठरी को गिराकार ध्वस्त कर दिया जाए और हृदय को 'एक में सब और सब में एक' वाले उदात्त सिद्धान्त के रूप में विराट् बनाया जाए। मानव की मानवता को यदि सही अर्थ में जीवित रहना है, तो वह विशाल, उदार, विराट, निःस्वार्थ एवं अनन्त की ओर उन्मुक्त निर्मल प्रेम के सहारे ही जीवित रह सकती है।
उदात्त एवं उदार प्रेम के पास केवल एक ही भाषा है-देने की, देते रहने की, हंसते हंसाते सर्वस्व लुटाते रहने की। सच्चा प्रेम लुटना पसन्द करता है। लूटना उसे बिल्कुल पसन्द नहीं है। हिमालय की बुलंदियों से भी कहीं अधिक बुलंदियों तक ऊंचा उठा हुआ यह सर्वस्व-दानी उदार प्रेम कृतघ्न नहीं होता। ऐसे प्रेम से कभी किसी की कोई शिकायत नहीं हो सकती। शिकायत उसी प्रेम से होती है, जो ऊपर से तो प्रेम का सुन्दर बाना पहने रहता है, किन्तु अन्दर में स्वार्थी होता है, खुदगर्ज होता है। स्वार्थ हर क्षण लेना ही लेना जानता। है देना ! सच्चे मन से देना, उसने कभी सीखा ही नहीं। वह दर-दर का कंगाल भिखारी है, ओढ़र दाता नहीं। ऐसा प्रेम ही कृतघ्न, बेवफा होता है। स्वार्थ की जरा भी कहीं ठोकर लगी नहीं कि बस 'यूयं यूयं, वयं वयम्' की संस्कृतोक्ति चरितार्थ
प्रेम का पुण्य पर्व
१६५
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org