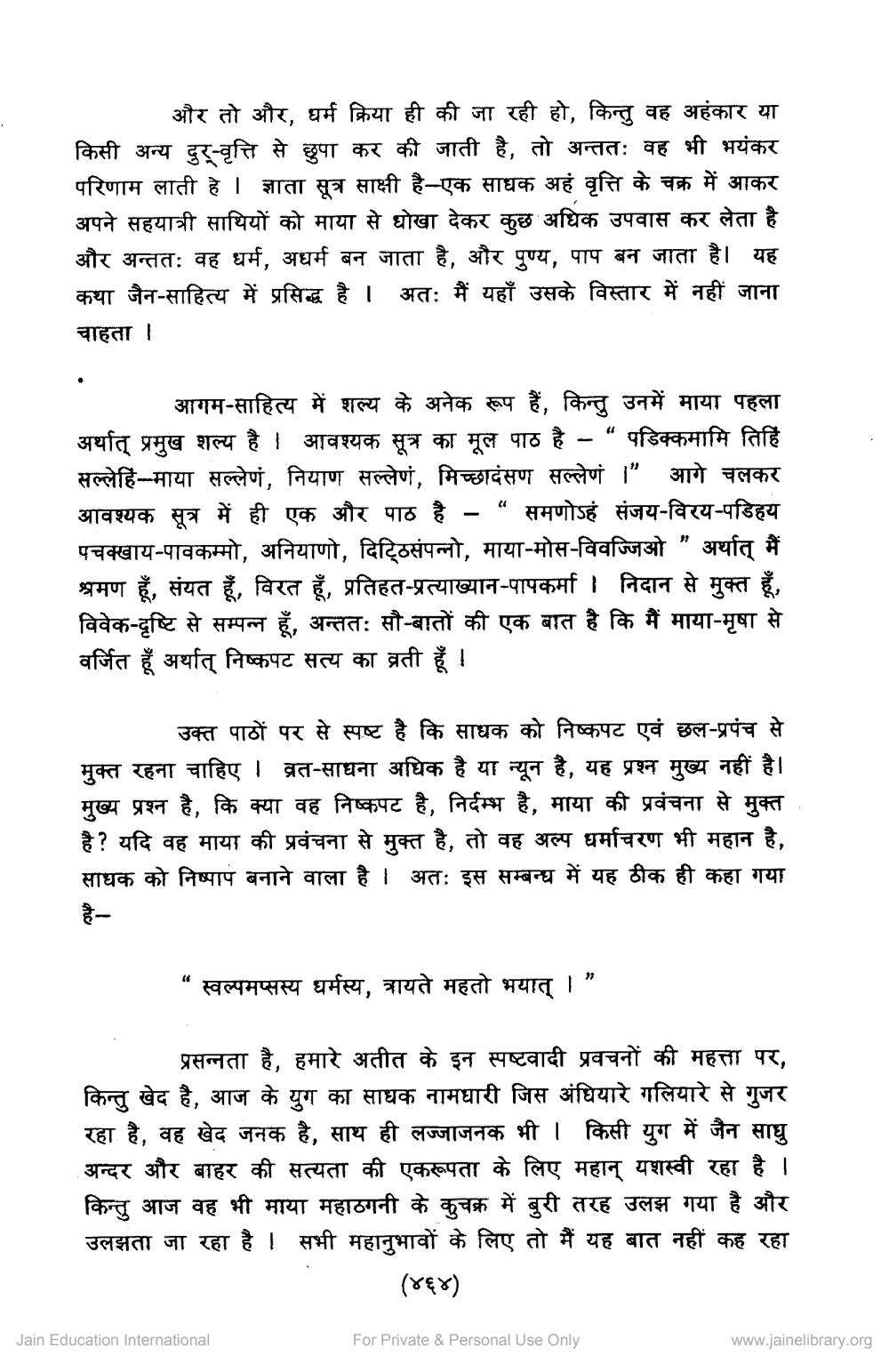________________
और तो और, धर्म क्रिया ही की जा रही हो, किन्तु वह अहंकार या किसी अन्य दुर्-वृत्ति से छुपा कर की जाती है, तो अन्ततः वह भी भयंकर परिणाम लाती है । ज्ञाता सूत्र साक्षी है - एक साधक अहं वृत्ति के चक्र में आकर अपने सहयात्री साथियों को माया से धोखा देकर कुछ अधिक उपवास कर लेता है और अन्तत: वह धर्म, अधर्म बन जाता है, और पुण्य पाप बन जाता है। यह कथा जैन - साहित्य में प्रसिद्ध है । अतः मैं यहाँ उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता ।
आगम - साहित्य में शल्य के अनेक रूप हैं, किन्तु उनमें माया पहला अर्थात् प्रमुख शल्य है । आवश्यक सूत्र का मूल पाठ है " पडिक्कमामि तिहिं सल्लेहि-माया सल्लेणं, नियाण सल्लेणं, मिच्छादंसण सल्लेणं । " आगे चलकर आवश्यक सूत्र में ही एक और पाठ है समणोऽहं संजय - विरय-पडिय पचक्खाय - पावकम्मो, अनियाणो, दिट्ठिसंपन्नो, माया - मोस - विवज्जिओ " अर्थात् मैं श्रमण हूँ, संयत हूँ, विरत हूँ, प्रतिहत प्रत्याख्यान - पापकर्मा । निदान से मुक्त हूँ, विवेक - दृष्टि से सम्पन्न हूँ, अन्ततः सौ- बातों की एक बात है कि मैं माया - मृषा से वर्जित हूँ अर्थात् निष्कपट सत्य का व्रती हूँ !
उक्त पाठों पर से स्पष्ट है कि साधक को निष्कपट एवं छल-प्रपंच से मुक्त रहना चाहिए । व्रत-साधना अधिक है या न्यून है, यह प्रश्न मुख्य नहीं है। मुख्य प्रश्न है, कि क्या वह निष्कपट है, निर्दम्भ है, माया की प्रवंचना से मुक्त है ? यदि वह माया की प्रवंचना से मुक्त है, तो वह अल्प धर्माचरण भी महान है, साधक को निष्पाप बनाने वाला है । अत: इस सम्बन्ध में यह ठीक ही कहा गया
है
"6
"
स्वल्पमप्सस्य धर्मस्य, त्रायते महतो भयात् ।
"
प्रसन्नता है, हमारे अतीत के इन स्पष्टवादी प्रवचनों की महत्ता पर, किन्तु खेद है, आज के युग का साधक नामधारी जिस अंधियारे गलियारे से गुजर रहा है, वह खेद जनक है, साथ ही लज्जाजनक भी । किसी युग में जैन साधु अन्दर और बाहर की सत्यता की एकरूपता के लिए महान् यशस्वी रहा है । किन्तु आज वह भी माया महाठगनी के कुचक्र में बुरी तरह उलझ गया है और उलझता जा रहा है । सभी महानुभावों के लिए तो मैं यह बात नहीं कह रहा
(४६४)
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org